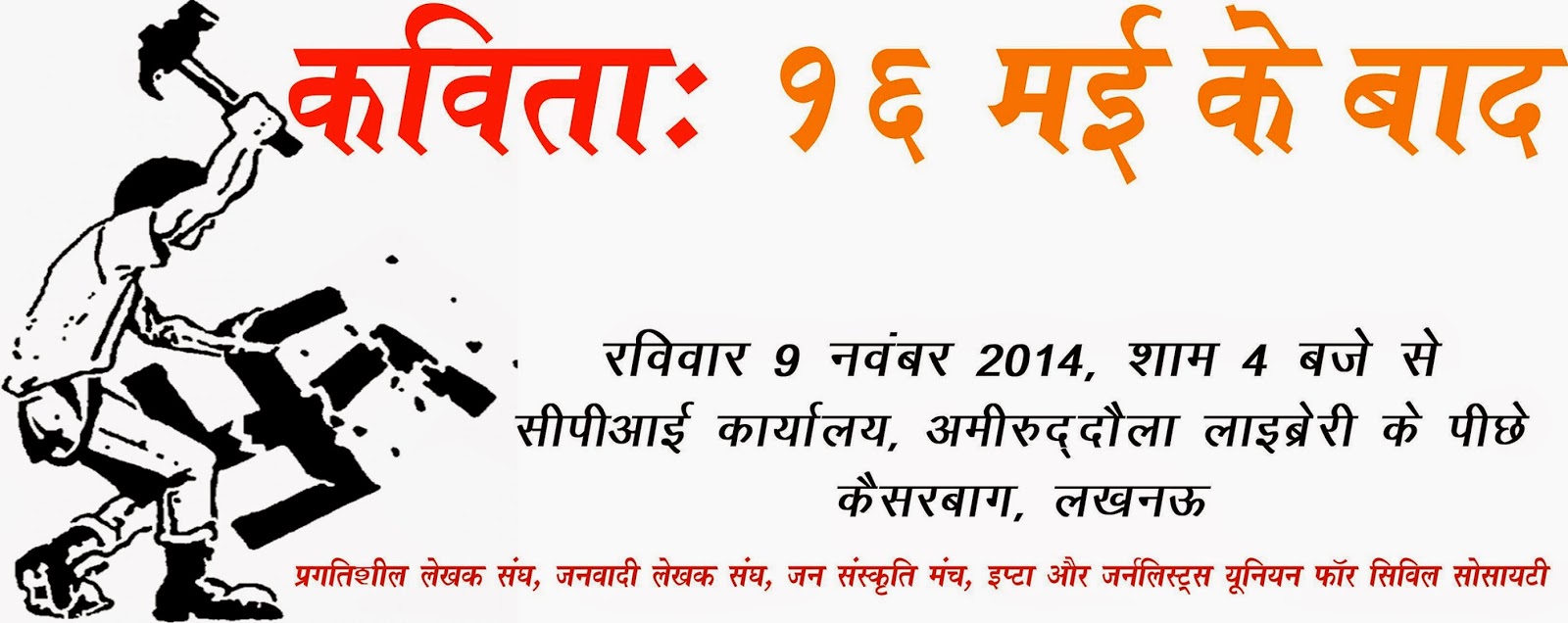-उमेश पंत
हैदर कश्मीर के भूगोल को अपनी अस्मिता का सवाल बनाने की जगह कश्मीरियों के मनोविज्ञान को अपने कथानक के केन्द्र में खड़ा करती है और इसलिये उसकी यही संवेदनशीलता उसे बाकी फिल्मों से अलग पंक्ति में खड़ा कर देती है। हैदर इन्तकाम के लिये इन्तकाम को नकारती एक फिल्म है। हैदर की सबसे खूबसूरत बात ये है कि उसमें मौजूद हिंसा भी, हिंसा के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है।
 +मैंजिन दिनों मुम्बई में रह रहा था मेरा एक रुम मेट कश्मीरी था। उसके पापा एक आईएएस ऑफिसर हैं। उन दिनों उसकी मां मुम्बई आई हुई थी। वो अक्सर खामोश रहती। मैं देर रात भर अपने कमरे में बैठा लिख रहा होता और वो चुपचाप किचन में बरतनों से जूझती रहती। कुछ देर बाद पूरे कमरे में खुशबू फैल जाया करती। उस खुशबू में कश्मीर बसा होता। खाना तैयार होने के बाद वो मुझे अपने कमरे में बुलाती और प्यार से मेरे मना करने के बावजूद मेरे लिये खाना परोस देती। एक दिन जब वो लड़का घर पे नहीं था मैं आंटी के पास बैठा उनसे कश्मीर के बारे में पूछ रहा था। आंटी कितनी खूबसूरत जगह में रहते हो आप। मेरे ये कहने पर वो कुछ देर चुप रही और फिर कश्मीर के हालात बयां करते हुए वो एकदम रुंआसी हो गई। बेटा 6 महीने कश्मीर रहने के बाद सबकुछ छोड़कर जम्मू आकर रहना पड़ता है। इतना डर डर के जीते हैं, कब क्या हो जाये कुछ पता नहीं। हर दसरे दिन कर्फ्यू। बच्चों को घर से बाहर भेजने में डर लगता है। ऐसे में कुछ खूबसूरत नहीं लगता। उन्होंने अपने कश्मीरी लहज़े में जो कहा था उसका सार यही था। बाद में पता चला कि वो पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन की गोलियां ले रही थी और मेरे उस कश्मीरी रुममेट ने बताया कि डिप्रेशन कश्मीर में खासकर महिलाओं में एक आम समस्या है।
+मैंजिन दिनों मुम्बई में रह रहा था मेरा एक रुम मेट कश्मीरी था। उसके पापा एक आईएएस ऑफिसर हैं। उन दिनों उसकी मां मुम्बई आई हुई थी। वो अक्सर खामोश रहती। मैं देर रात भर अपने कमरे में बैठा लिख रहा होता और वो चुपचाप किचन में बरतनों से जूझती रहती। कुछ देर बाद पूरे कमरे में खुशबू फैल जाया करती। उस खुशबू में कश्मीर बसा होता। खाना तैयार होने के बाद वो मुझे अपने कमरे में बुलाती और प्यार से मेरे मना करने के बावजूद मेरे लिये खाना परोस देती। एक दिन जब वो लड़का घर पे नहीं था मैं आंटी के पास बैठा उनसे कश्मीर के बारे में पूछ रहा था। आंटी कितनी खूबसूरत जगह में रहते हो आप। मेरे ये कहने पर वो कुछ देर चुप रही और फिर कश्मीर के हालात बयां करते हुए वो एकदम रुंआसी हो गई। बेटा 6 महीने कश्मीर रहने के बाद सबकुछ छोड़कर जम्मू आकर रहना पड़ता है। इतना डर डर के जीते हैं, कब क्या हो जाये कुछ पता नहीं। हर दसरे दिन कर्फ्यू। बच्चों को घर से बाहर भेजने में डर लगता है। ऐसे में कुछ खूबसूरत नहीं लगता। उन्होंने अपने कश्मीरी लहज़े में जो कहा था उसका सार यही था। बाद में पता चला कि वो पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन की गोलियां ले रही थी और मेरे उस कश्मीरी रुममेट ने बताया कि डिप्रेशन कश्मीर में खासकर महिलाओं में एक आम समस्या है।कल हैदर देखते हुए हैदर की मां की आंखों में भी वही डर साफ दिखाई दिया था। अपनी ही धरती से कौन कब किसकी जिन्दगी से कैसे गायब कर दिया जाएगा, जो लोग ताजि़न्दगी इस डर के साये में जी रहे होंगे… जब हमें उनकी जि़न्दगी की कल्पना से भी डर लगने लगता है तो उनके डर की कल्पना तो हम कर भी नहीं सकते। और अक्सर कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हमारी मुख्यधारा की फिल्मों को वो डर यथार्थ का हिस्सा ही नहीं लगता और उनकी कल्पनाएं उस डर तक कभी पहुंच ही नहीं पाती।
हैदर उन विरली फिल्मों में से एक है जो उस डर का भी पक्ष सामने रखती है जिसे अक्सर राष्ट्रभक्ति की दीवार खड़ी करके सिनेमाई परदों के हासिये पर डाल दिया जाता है। जिस पर अन्ततः राष्ट्रभक्ति का चश्मा हावी हो जाता है जिसका हासिल कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे से आगे कुछ नहीं होता।
हैदर कश्मीर के भूगोल को अपनी अस्मिता का सवाल बनाने की जगह कश्मीरियों के मनोविज्ञान को अपने कथानक के केन्द्र में खड़ा करती है और इसलिये उसकी यही संवेदनशीलता उसे बाकी फिल्मों से अलग पंक्ति में खड़ा कर देती है। हैदर इन्तकाम के लिये इन्तकाम को नकारती एक फिल्म है। हैदर की सबसे खूबसूरत बात ये है कि उसमें मौजूद हिंसा भी, हिंसा के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है।
लालचौक पर खड़ा हैदर गरदन पर रेडियो टांगे जब इस पार और उस पार की आज़ादी के नारे बुलंद कर रहा होता है तो उसे घेरकर खड़ी भीड़ में मुझे अपने उस कश्मीरी रुममेट की मां का चेहरा भी किसी एक कोने में खड़ा नज़र आता है।
हैदर की मां गजाला दरअसल हालातों में पिसने की जगह हालातों से समझौता कर लेती एक औरत है। वो अपने डाॅक्टर पति डा हिलाल मीर के साथ रहते हुए सुरक्षा के अभाव को अपने लिये अपने देवर खुर्रम (के के मेनन) के आकर्षण से कहीं संतुलित कर लेने की कोशिश करती है। लेकिन जब उस देवर को अपने ही बेटे को खत्म कर देने का प्रण लेते देखती है तो जैसे उस संतुलन की ज़मीन खिसक जाती है। वो एक मां के रुप में अन्दर तक हिल जाती है। उसी के शब्दों में एक मां के लिये उसके बेटे को खो देने से बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। ‘आधी विधवाओं’ के दर्द को ही नहीं बल्कि उनके मनोविज्ञान की गहराइयों को, उनकी असुरक्षा को, अपनी सन्तानों और परिवारों के लिये उनके भय को, और प्यार और आकर्षण जैसे सहज मानवीय व्यवहारों को प्रतीकों की ढ़ाल में बयां कर देता है गज़ाला का ये किरदार।
हैदर के रुप में शाहिद कपूर करिश्माई हैं। उन्होंने अपने किरदार में एक एक इंटलेक्चुअल कवि, एक नटखट प्रेमी, अपने गायब कर दिये गये बाप की तलाश में भटकते एक फितूरी बेटे, अपनी मां और चाचा के बीच पनपते रिश्ते से खफा एक सन्तान और एक विद्रोही सभी भूमिकाओं में ऐसा सन्तुलन बनाया है कि वे हैदर के रुप यादगार हो जाते हैं। खासकर मंच पर जब वो बुलबुल-ए-बिस्मिल का नाटकीय मंचन कर रहे होते हैं तो उनके अभिनय की पराकाष्ठा देखने को मिल जाती है। लाल चौक पे हज़ारों कश्मीरियों को चुत्स्पा का मतलब समझाते हुए और अपनी आज़ादी की गुहार लगाते हुए वो बेहतरीन अभिनय करते हैं।
बर्फ की सफेद दुनिया के बीच से रुहदार के किरदार में इरफान खान का पहला अपेयरेंस ही इतना दमदार है कि वो पहली ही नज़र में अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। उनकी उपस्थिति भर से फिल्म एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। श्रद्धा कपूर भी अशिर्या के किरदार में बहुत भोली लगती हैं।
‘हैदर’ का हर एक किरदार तो मर्मस्पर्शी प्रतीक गढ़ता ही है पर कई बार ये भी होता है कि कश्मीर के भूगोल के हिस्से भी फिल्म में प्रभावशाली किरदारों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। वो किनारा ढूंढ़ती झेलम हो या अपनी आज़ादी मांगते कश्मीरियों से घिरा लालचौक। डाउनटाउन के पुल के दूसरी ओर हथियार बंद लोगों से घिरी तंग गलियां हो या फिर वो कब्रें जिनमें दफ्न लोगों की पहचान उनपर लिखे अंकों से होती है। वो बर्फीली ज़मीन भी जहां तीन बुजुर्ग अपने लिये कब्रें खोद रहे हैं। और सबसे प्रभावशाली वो घर जिसे वक्त के एक हिस्से में तोप से उड़ा दिया जाता है और जहां अब यादों के जले हुए हिस्से अपनी पूरी टूटन के साथ बिखरे हुए हैं। फिल्म में मौजूद भूगोल के ये हिस्से तब भी लगातार कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं जब फिल्म में किरदार बोल नहीं रहे होते। इनके मूक संवाद फिल्म देखने के कई देर बाद तक भी ज़हन के कोंनों में कुछ कुछ बोलते रहते हैं।
जब हम ‘कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है’ कहकर कश्मीर के लोगों की राय जानने को राष्ट्रदोह के नज़रिये से देखने लगते हैं तो हमारी चेतना उन बर्फीली कब्रों में दफन हो गई सी लगती है जिन्हें कश्मीर की आवाम खुद अपने लिये खोदने को मजबूर है। विशाल भारद्वाज अपनी इस फिल्म में उस चेतना को कई बार पटकनें देते हैं। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम जैसे अमानवीय कानून को चुत्स्पा के जुमले में लपेटकर उसकी भद्द पीटते हुए या फिर फिल्म के को-राइटर बशरत पीर द्वारा निभाये गये उस किरदार के रुप में जो अपने घर में इसलिये नहीं घुस रहा क्योंकि उसकी तलाशी नहीं ली गई, या फिर उन तीन बजुर्गाें के किरदारों के रुप में जो अपने लिये खुद कब्र खोद रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज नही तो कल उनका यही हश्र होना है, फिल्म इन प्रतीकों के रूप में तीखे तंज़ भी कसती है जो सीधे दिल पर असर करते हैं।
फिल्म कुछ हिस्सों में ज़बरदस्ती खिंचती भी मालूम होती है। अर्शिया का सदमा, सलमान और उसके भाई के किरदार से फिल्म में हास्य उकेरने की कोशिश और आंखिर में गज़ाला का आत्मघाती हो जाना, फिल्म में ज़बरदस्ती का मैलोड्रामा डालने की कोशिश लगता है और उसके स्तर पर कुछ नकारात्मक सा असर डालता है।
फिल्म जब पूरी हो जाती है तो उसके कई दृश्य दिमाग में रह जाते हैं लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि कोई एक स्पष्ठ संदेश तुरंत याद नहीं आता। हैदर के पिता का हैदर के लिये संदेश फिल्म में लगभग तीन बार दोहराया गया है। जिसमें वो कहते हैं कि मेरा इन्तकाम लेना। और गज़ाला का फैसला ऊपर वाले पर छोड़ देने की बात भी एक बार की गई है। तो ऊपर वाला गज़ाला के लिये इस तरह का फैसला क्यों लेता है ये बात गले नहीं उतरती। खुर्रम के दोनों पैर आंखिर में कटे हुए हैं वो मौत के एकदम करीब है ऐसे में उसे उसके हाल पे छोड़ देना उसने मर जाने से भी कठिन यातना देने की तरह है। ये तो इन्तकाम का चरम है कि जहां कोई इस हाल में है कि वो मरने की भीख मांग रहा है और आप उसे मौत भी नसीब नहीं होने देते।
ये अगर एक पीरियड फिल्म है तो डिसअपेयरेंस की त्रासदी को तो फिल्म छूंती है लेकिन कश्मीरी पंडितों का नेरेटिव फिल्म में कहीं नज़र नहीं आता। इस लिहाज़ से फिल्म कुछ मायनों में असंतुलित भी नज़र आती है।
खैर जहां फिल्म कमज़ोर पड़ती है वहां उसे गुलज़ार के लफ्ज़ों और विशाल भारद्वाज का संगीत बांध देता है और फिर कश्मीर भी तो इतना खूबसूरत है कि वहां यातनाएं भी खूबसूरती के कपड़े पहनी हुई मालूम होती हैं। शायद यही वजह कि वो यातनाएं उन्हें दिखाई ही नहीं देती जो बस ऊपरी तौर पर कश्मीर का सच जानने की कोशिश करते हैं। जो रुह तक पहुंचते हैं वो खूबसूरती के साथ साथ दर्द भी महसूस कर पाते हैं।
एक खूबसूरत दुनिया जहां रह रहे लोगों का मूलभूत सवाल ही ये है कि “मैं हू या मैं नहीं हू”, उस दुनिया में रह रहे लोगों के अस्तित्व की लड़ाई को समझने की एक समझदार कोशिश हैदर ज़रुर करती है।