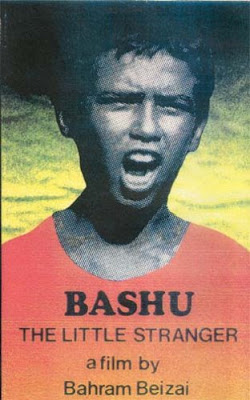"...यह रिएक्टर प्लांट भले ही भारत के शहरों को रोशनी दे लेकिन इस गांव के भविष्य को अंधेरे में डुबो दिया है. दूसरे को रोशन करने के लिए जिन लोगों की ज़मीन गई, घर गया उनको मिला तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बीमारी..."
अब तक वहां पर छः परमाणु रिएक्टर बन कर चालू हो चुका है. रिएक्टर सात और आठ का काम चालू है.
रिएक्टर नं. एक 2014 से बंद है, बाकी 5 रिएक्टर से करीब 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है. इसके आस-पास थमलाव, झरझनी, दीपपुरा, मालपुरा, बक्षपुरा जैसे और कई छोटे-बड़े गांव हैं जिसकी परमाणु रिएक्टर से एरियल दूरी 5-6 किमी के अन्तर्गत है.
इस क्षेत्र की आबादी मुख्यतः खेती और मजदूरी पर निर्भर है. यहां का मुख्य उपज मक्का, सोया, ज्वार-बाजरा है. शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है. इन ईलाकों से बहुत कम लोग ही राजस्थान से बाहर काम के लिये जाते हैं.
यहां पर आधी आबादी के पास घर के नाम पर एक झोपड़ी है और चौथाई के पास समान के नाम पर घर में एक या दो टूटी हुई खाट है. खासकर भील समुदाय की स्थित बहुत ही दयनीय है.
थमलाव के शैलेन्द्र बताते हैं कि यहां परमाणु रिएक्टर बन रहा था तो लोग खुश थे कि इससे उनको रोजगार मिलेगा. उस समय तक लोगों में परमाणु रिएक्टर से होने वाले नुकसान की भी जानकारी नहीं के बराबर थी.
लोगों ने इसलिए शुरूआती दिनों में इसको खुशी-खुशी अपनाया. परमाणु रिएक्टर बन कर चालू हुआ, बिजली बनने लगे लेकिन उसमें गांव वालों को स्थायी रोजगार नहीं मिला.
जब रिएक्टर तीन और चार बन रहा था तब भी गांव वालों को आशा थी कि इनमें स्थायी रोजगार मिलेगा. तीन और चार रिएक्टर चालू हो गया लेकिन इनमें भी गांव वालों को रोजगार नहीं मिला.
दस सालों में रिएक्टर से निकलने वाले रेडियेशन से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ने लगा. लोगों में कई तरह की नई-नई बीमारी फैलने लगीं. काम करते हुए कई लोग रेडियेशन की चपेट में आ गये और उनकी मृत्यु हो गई.
रिएक्टर पांच और छः बनना शुरू हुआ तो लोग संगठित होकर परमाणु विद्युत संयत्र के खिलाफ आवाज उठाने लगे. पांच और छः रिएक्टर भी 2010 में शुरू हो गया और लोगों को स्थायी काम नहीं मिला.
उनको ठेकेदारी के तहत ही रिएक्टर में काम मिल पाया. अब गांव के और नजदीक रिएक्टर सात और आठ बन रहा है जिससे थमलाव गांव के लोगों में डर है कि वे विस्थापित हो जाएंगे.
रिएक्टर के आस-पास के गांव वालों के लिए यहां पर बेलदारी, ड्राइबरी, मिस्त्री, बेलडर, हेल्फर इसी तरह का काम मिलता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों जाते हैं.
इन गांवों की दो पीढि़यां इसी तरह की काम करती आई हैं लेकिन उनको स्थायी रोजगार नहीं मिला. चालू प्लांट में कुछ लोगों को नौकरी मिली भी तो ठेकेदारी के तहत. वे वर्षों से काम करते आये है लेकिन आज तक उनको स्थायी नहीं किया गया.
ठेकेदार बदल जाते हैं लेकिन मजूदर वही रहते हैं. इन ठेकेदारी मजदूरों की मजदूरी कम होती है लेकिन सबसे खतरनाक काम इनसे करवाया जाता है. प्लांट के अन्दर जब कोई रिएक्टर शट डाउन होता है (जब रिएक्टर में बिजली उत्पादन रोककर मशीनों, कचरों की सफाई होती है) तब मजदूरों की मांग और बढ़ जाती है.
उस समय मजदूरों को थोड़ा ज्यादा पैसा देकर (200 रू. की जगह 300 रू. या 7000 रू. प्रति माह की जगह 10000 रू. प्रति माह) उनसे जरूरत से ज्यादा समय तक काम करवाया जाता है.
अगर कम्पनी द्वारा 30 मिनट अन्दर रहकर काम करवाने की परमिट दी जाती है तो ठेकेदार उसको 90 से 100 मिनट काम करने के लिए बाघ्य करते हैं. कम्पनी द्वारा टी.एल.डी., डोजो मीटर दिया जाता है जिससे उनको पता चल सके कि कितने खतरे पर काम करते हैं.
उसको अन्दर जाने से पहले एयर लॉक पर ठेकेदार का सुपरवाईजर इस मशीन को ले लेता है. एन.पी.सी.एल. (न्यूक्लियर पॉवर कारपारेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड) का सुपरवाईजर बाहर ही रूक जाता है.
टी.एल.डी. की रीडिंग के लिए बाम्बे भेजा जाता है. रीडिंग के बाद कभी भी मजदूरों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है. थमलाव के राजकुमार बताते हैं कि वे रिएक्टर 5-6 में 6 साल से काम कर रहे हैं जहां पर उनको 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा मिलता है. वे बताते हैं कि जहां ज्यादा रेडियेसन होता है वहां रबड़ और प्लास्टिक का गलप्स और सूट पहन कर जाना होता है. इस सूट को पहनने से काम की स्पीड कम होती है तो ठेकेदार का सुपरवाईजर दबाव देता है कि गलप्स खोल कर काम करो. इस तरह काम करते हुए कई मजदूर रेडिएशन के शिकार हुये और उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई.
ऐसी ही एक घटना थमलाव के सिक्ख परिवार में हुई जिसको रेडियेशन लगने के बाद कम्पनी व ठेकेदार द्वारा अस्पताल नहीं जाने दिया गया. उसको घर भेज दिया गया और 3-4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई.
यह घटना कहीं दर्ज नहीं हुई, न ही उस पीडि़त परिवार को कोई मुआवजा दिया गया. इसी पीडि़त परिवार का एक लड़का कम्पनी के अन्दर एक्सीडेंट में मारा गया. इसी तरह की घटना कम्पनी के अन्दर आये दिन घटती रहती है. 23 जून, 2012 को प्लांट के अन्दर रिसाव होने से 38 मजदूर रेडिएशन के शिकार हो गये.
प्रेमशंकर, जिनकी उम्र 24 साल है, झरझनी गांव के रहने वाले हैं. वह 2010 में प्लांट नं. 5-6 में ठेकेदार ललित छाबड़ा के पास सफाई का काम किये. प्रेमशंकर को उस समय 73 रू. प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती थी.
उसको छोड़कर वह प्लांट 7-8 में हिम्मत सिंह ठेकेदार के पास हेल्फर का काम करने लगे, जहां उनको 165 रू. मिलती थी. 7 फरवरी, 2012 को प्रेमशंकर नियमित समय से जाकर अपने काम पर लगे थे कि कुछ समय बाद अचानक 36 एम.एम. का सरिया 20 फूट की उंचाई से उनके ऊपर आ गिरा. सरिया गिरते ही काम कर रहे दूसरे मजदूरों को पता चल गया. मजदूरों को आनन-फानन में छुट्टी कर दिया गया.
प्रेमशंकर भाग्यवान थे कि उनको यह सरिया सिर पर नहीं लगी, नहीं तो यह सरिया उनकी जान ले सकता था.
उनको यह सरिया दांये कंधे के नीचे पीठ पर लगी जिससे वह अचेत हो गये. उनको उठा कर कम्पनी के अन्दर डिस्पेन्सरी में ले जाया गया, जहां पर दर्द निरोधक दवा देकर रावत भट्टा के लिए रेफर कर दिया गया.
रावत भट्टा में कुछ समय रख कर उनको कोटा रेफर कर दिया गया, जहां पर एक माह तक वह एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहे. प्रेमशंकर को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया. मुआवजा के बदले उनको यह कहते हुए काम से ही निकाल दिया गया कि अब इससे काम नहीं हो सकता. प्रेमशंकर ने कई बार ठेकेदार और सुपरवाईजर से मिलने की कोशिश की लेकिन उनको गेट पास ही नहीं दिया गया.
इस तरह कम्पनी मजदूरों को विकलांग बनाकर काम से बाहर निकाल देती है. प्रेमशंकर बताते हैं कि छोटी-मोटी घटना तो वहां महीने में दो-चार होती ही रहती है, कभी-कभी इससे बड़ी घटना भी होती है. वह बताते हैं कि लोकल थे इसलिए कम्पनी ने उनका ईलाज भी करवा दिया.
बाहरी लोगों को कम्पनी ईलाज नहीं करवाती और गम्भीर चोट लगने पर उनको गायब भी कर देती है. 27 मई, 2015 को मोहम्मद अकरम को मार-पीट कर ठेकेदार ने कम्पनी से निकाल दिया जिसकी लिखित शिकायत अकरम ने रावत भट्टा पुलिस स्टेशन में की है.
सामाजिक सरोकार दायित्व के तहत एन.पी.सी.एल. ने गांव में दो या तीन सोलर लैम्प लगवा कर अपनी सामाजिक दायित्व की इति श्री कर ली है. बंजारा बस्ती वन के गंगा राम करीब 20 साल से इस रिएक्टर में काम करते हैं. पहले वह 3-4 में हेल्पर का काम किया, फिर वेल्डर बन गये और अब वह रिएक्टर 7-8 में हिन्दुस्तान कंट्रेक्टर कम्पनी में सुपरवाईजर का काम करते हैं जिसके लिए उन्हें 395 रु. मिलता है.
गंगा राम बताते हैं कि एन.पी.सी.एल. रावत भट्टा परमाणु बिजलीघर ने थमलाव के बंजरा बस्ती वन और टू को नवम्बर 2003 से गोद लिया हुआ है. इन दोनों बस्तियों को मिलाकर करीब 130-140 घर बंजारा समुदाय का है.
एन.पी.सी.एल. ने 11 साल बाद सितम्बर 2014 में सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए 1500 मीटर लम्बा सीमेंट-कंक्रीट सड़क का निर्माण बंजरा बस्ती में किया है.
बंजारा बस्ती वन में शिक्षा के नाम पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जहां पर गांव के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं. आगे की पढ़ाई के लिए दो कि.मी. दूर थमलाव जाना पड़ता है, जहां पर आठवीं तक की पढ़ाई होती है.
आठवीं के बाद अगर पढ़ाई जारी रखना है तो रावत भट्टा जाना पड़ता है, जहां आने-जाने के लिए माता-पिता को 30-40 रू. रोज खर्च करने पड़ते हैं. यही कारण है कि आज तक बंजारा बस्ती वन की कोई लड़की दसवीं तक पढ़ाई नहीं कर पायी है.
कुछ ही लड़के रावत भट्टा जाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं. एन.पी.सी.एल. ने इस गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं खोला. स्वास्थ्य की हालत यह है कि करूणा ट्रस्ट बंगलौर की सप्ताह में एक दिन दो घंटे के लिए एक मोबाइल डिस्पेनसरी आती है.
गम्भीर बीमारी होने पर उनको रावत भट्टा या कोटा खुद के खर्चे पर ईलाज कराना पड़ता है. एन.पी.सी.एल राजस्थान के पास 85 बेड का अस्पताल रावत भट्टा में है. इस अस्पताल में केवल स्थायी कर्मचारियों का ही ईलाज होता है.
गोद लिये हुए गांव के किसी व्यक्ति या ठेकेदारी पर काम कर रहे मजदूरों का ईलाज नहीं किया जाता है.
एन.सी.पी.एल द्वारा 14 फरवरी, 2005 को बंजारा बस्ती एक में विद्युतीकरण किया गया. लेकिन इस गांव में बिजली की वही हालत है जो कि और गांवों में है. इस बस्ती के लोगों को बिजली बिल का राजस्थान के अन्य गांव जैसे ही भुगतान करना पड़ता है.
बिजली की कटौती होती है. खेत के लिए पम्पिंग सेट चलाना है तो रात में वोल्टेज मिलता है तभी चलाया जा सकता है. खेतों को पानी देने के लिए एक तलाब है जो थमलाव गांव के सरपंच का है.
इस तलाब से पानी लेने के लिए फसल का आधा पैदावार या 100 रू. प्रति घंटा के हिसाब से भुगतान करने पर खेत को पानी मिलता है. पीने के पानी के लिए गांव से बाहर एक टब लगा हुआ है उससे ही गांव वालों को पानी लाना पड़ता है.
इसी तरह की हालत उस इलाके के सभी गाँवों के हैं. पीने के पानी के लिए हर गांव में एक या दो टब होते हैं जहां पर एक से दो घंटे ही पानी आता है. पानी लेने के लिए घंटों पहले से लाईन में लगाना होता है तब जाकर कहीं पानी मिलता है.
राणा प्रताप सागर बांध कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर है जहां पानी की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन इससे इन गांव को पानी नहीं मिलता है. गांव के लोगों का कहना है कि पानी जो आता है वह अच्छा नहीं होता है.
नंदा देवी के पति कृष्णा गेमन इंडिया लिमिटेड में ड्राइवर हैं लेकिन उनको हेल्फर का पैसा मिलता है. नंदा देवी के दो बच्चे हैं जो अनपढ़ हैं. लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं. वह चाहती हैं कि गांव में स्कूल और अस्पताल खोला जाये ताकि वे अपने बेटी और बेटे को पढ़ा सकें.
थमलाव की काफी महिलाएं 7-8 नम्बर रिएक्टर में बेलदारी का काम किया करती हैं. ये महिलाएं घर का काम करके सुबह 8 बजे घर से निकलती है और शाम 6.30 बजे के करीब घर को आती हैं.
घर पर आकर उनको घर का काम निपटाना होता है. इन महिलाओं को 200 या 250 रू0 मजदूरी मिलती है लेकिन इन को कोई छुट्टी नहीं दी जाती है. इन महिलाओं में खून और आयरन की कमी अधिक मात्रा में है.
एन.पी.सी.एल. रावत भट्टा परमाणु बिजलीघर को पानी पहुंचाने के लिए करीब 75 गांवों को डुबोकर 177 फीट ऊंचा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया. इस डूब क्षेत्र के लोग इधर-उधर बिखर गये लेकिन उनमें से करीब 100-150 परिवार झरझनी गांव में रह रहे हैं.
इसमें से बहुतों को मुआवजा तक नहीं मिला. परिवार में एक भाई को मुआवजा मिला तो दूसरे को नहीं. इसमें से अधिकांश लोग रावत भट्टा में बेलदारी का काम कर रहे हैं. इस प्लांट के आस-पास के सभी गांव वालों का कहना है कि सुबह उठने पर पूरे शरीर में दर्द होता है, सामान्य होने में करीब एक घंटा लगता है.
इस परमाणु बिजलीघर से न तो उनको बिजली 24 घंटे मिलती है और न ही पीने के लिए पानी मिलता है.
यह रिएक्टर प्लांट भले ही भारत के शहरों को रोशनी दे लेकिन इस गांव के भविष्य को अंधेरे में डुबो दिया है. दूसरे को रोशन करने के लिए जिन लोगों की ज़मीन गई, घर गया उनको मिला तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बीमारी.
एक बार उजड़े, फिर उजड़ने का डर सता रहा है. इनके बच्चों के भविष्य संवारने के लिए स्कूल, अस्पताल की जगह उनको एक ऐसा उपहार मिला है जहां कभी दुर्घटना हो तो उनका भविष्य ही नहीं बचेगा. पानी में उनके गांव को डूबो दिया गया लेकिन पीने को पानी नहीं है. दूसरे को रोशन करने वाले अंधेरे में क्यों रे भाई!